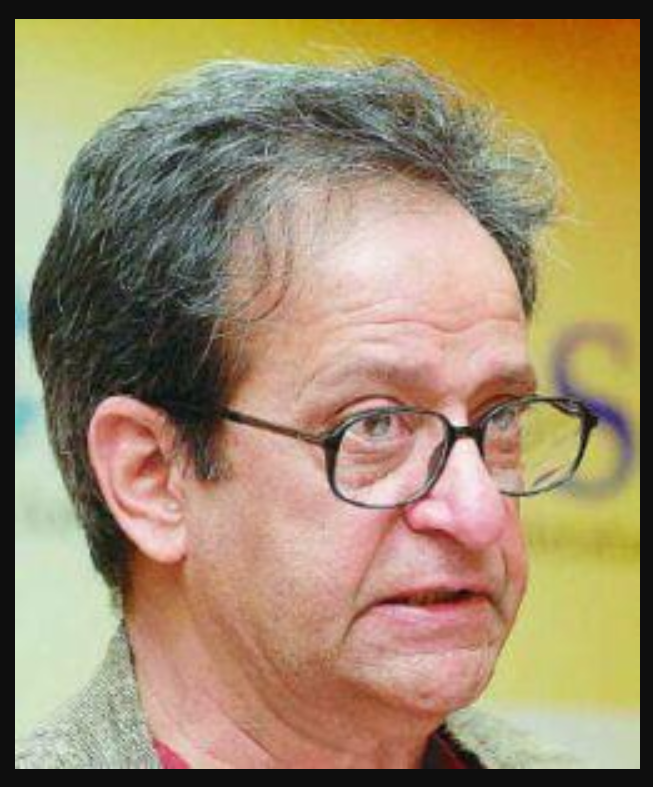सांस्कृतिक क्षेत्र के तीन मूलभूत परिवर्तन: एजाज़ अहमद
तीसरी दुनिया के देशों के साहित्य को राष्ट्रीय रूपक के बतौर नहीं देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ‘तीसरी दुनिया का साहित्य’ कहना ही अपने आप में एक पक्षपोषक/दुर्भावना-पूर्ण पद है। भारतीय साहित्य अपने आपद-धर्म में ही उपनिवेशवाद-विरोशी है। इसे राष्ट्रीय रूपक के बतौर देखना इसकी उपनिवेशवाद-विरोधी चेतना को कुंद करके सांप्रदायिक स्पर्श देना होगा। उत्तरऔपनिवेशक अध्ययन-पद्धति को इसी रूप में देखा जा सकता है।
ये सार-निष्कर्ष एजाज़ अहमद के हैं। वे भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख मार्क्सवादी बौद्धिक रहे हैं।
तीन मूलभूत परिवर्तन
By एजाज़ अहमद
पिछले दशक के दौरान सांस्कृतिक क्षेत्र में तीन मूलभूत परिवर्तन घटित हुए. पहला, हिंदुत्ववादी ताकतों का उभार हुआ, जिसके तहत जो शक्तियां राष्ट्रीय आंदोलन एवं गणराज्य बनने के प्रारंभिक दशकों के दौरान हाशिए पर पड़ी शक्तियां थी, अब भारत में (विशेषकर उत्तर भारत में) राजनीतिक प्रभुत्व एवं सांस्कृतिक वर्चस्व हासिल करने के प्रमुख दावेदार के तौर पर विद्यमान है.
दूसरा, आर्थिक उदारीकरण ने वस्तु पूजा की अखिल भारतीय संस्कृति के निर्माण की गति को प्रचंड रूप से तीव्र कर दिया, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे बुर्जुआवर्ग के शहरी परिवेश से निकलकर दूर-दराज़ के देहाती इलाक़ों तक फैल चुका है. साथ ही गणराज्य की स्थापना के मूलभूत सिद्धांतों पर किए जा रहे दूरगामी प्रभाव वाले आक्रमणों ने रोज़मर्रा के सांस्कृतिक जीवन का भयंकर पाशवीकरण किया है. समृद्धों की दैनंदिनिक संस्कृति का पाशवीकरण तो निश्चित रूप से हुआ ही है, ज़मीन पर विचर रहे संतुष्ट एवं असंतुष्ट लिप्साओं के प्रेत ने वृहत्तर समाज पर भी दूरगामी प्रभाव डाला है.
तीसरा, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय परियोजना का भाव, सामाजिक कल्याण के निर्णायक मध्यस्थ के तौर पर बाज़ार की सर्वोच्चता का स्वीकार एवं प्रतिस्पर्धा धार्मिकताओं के पूर्ण पण्यीकरण ने मिलकर जाति एवं संप्रदाय की बर्बर अस्मिताओं की नई फसल तैयार कर दी है. इन्हें स्वदेशवादी विद्वानों के मध्य बौद्धिक सम्मान प्राप्त है, जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता आधुनिकता का अभिशाप है, जबकि बर्बर अस्मिताएं कथित तौर पर ‘परंपरा’ के मूल तत्व है. इनमें से स्वदेशीवाद ‘उच्च संस्कृति’ की ख़ास किस्म की विकृति के तौर उभर रही है एवं हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्ष लोकाचार के समक्ष पैदा होने वाला सर्वाधिक आसन्न ख़तरे के रूप में उपस्थित है, किंतु सबसे बड़ा और दीर्घकालीन ख़तरा बाजार की बंदिगी को लेकर है जो अभी ‘उदारीकरण’ के झंडे तले किया जा रहा है. धन के बेपनाह सकेंद्रण और दरिद्रता के भयावह विस्तार के साथ संबंद्ध इस बहुसांस्कृतिक समाज में अनियंत्रित बाज़ार को उन्मुक्त छोड़ देना, अपने जात के ही • मुखालिफ खड़ी, ऐसी पाशविकृत हो चुकी संस्कृति के निर्माण की आशंका जगाती है। जो ‘संपूर्ण जीवन पद्धति’ के तौर पर संस्कृति के जरा भी भावबोध से बिलकुल विच्छित्र होगी और मूलगामी समता के स्वप्नों के साथ पैदा हुए गणराज्य के इस तरह के पाशवीकरण से ना ही राजनैतिक लोकतंत्र और ना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की संविदा पार पा सकेगी.
अनुवादक: मनोज झा
पुस्तक: किसकी सदी, किसकी सहस्त्राब्दी