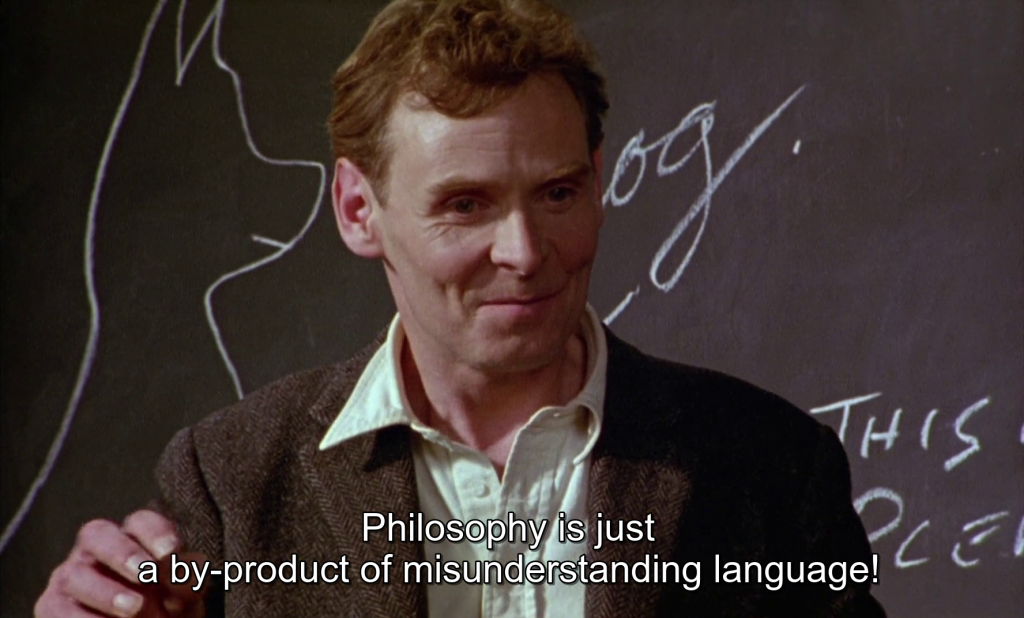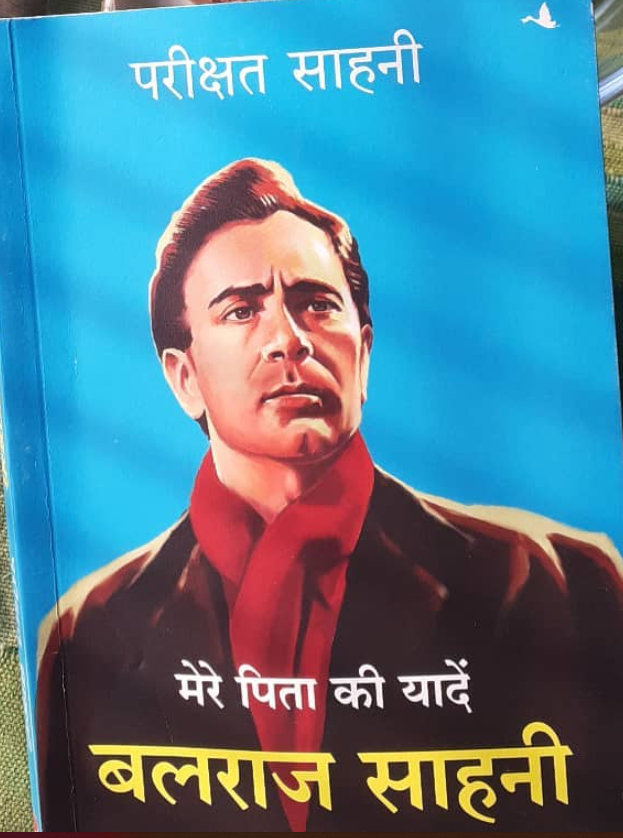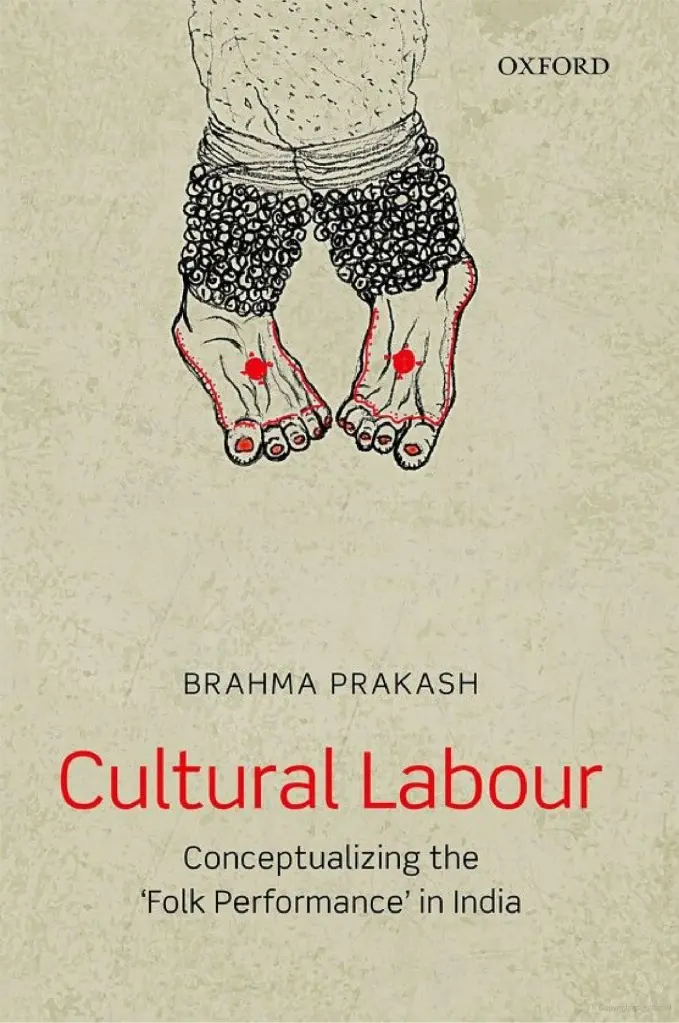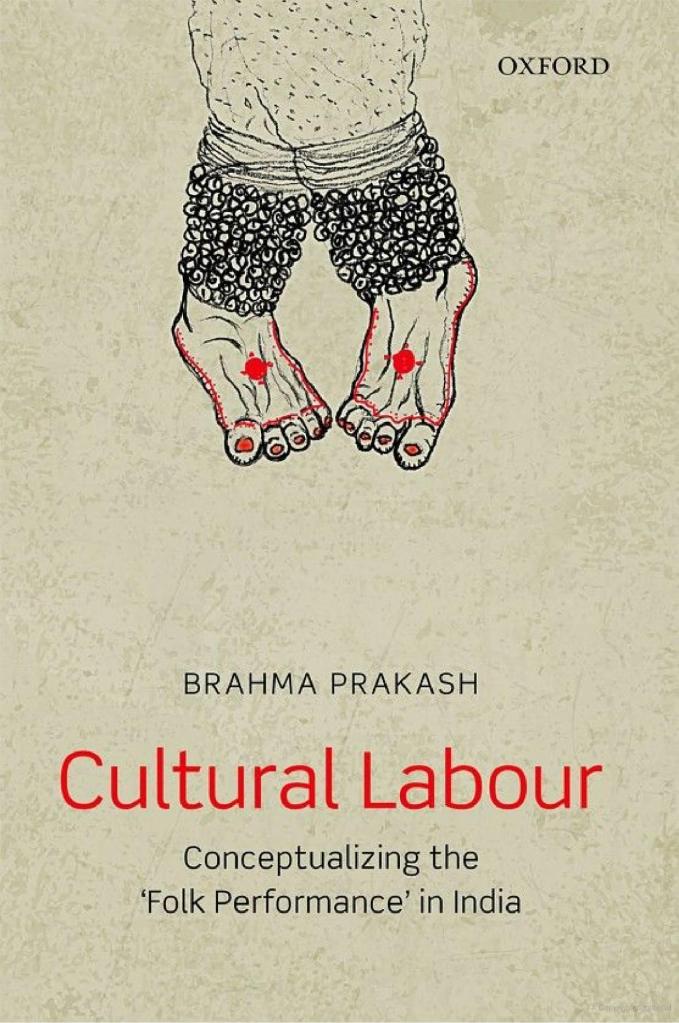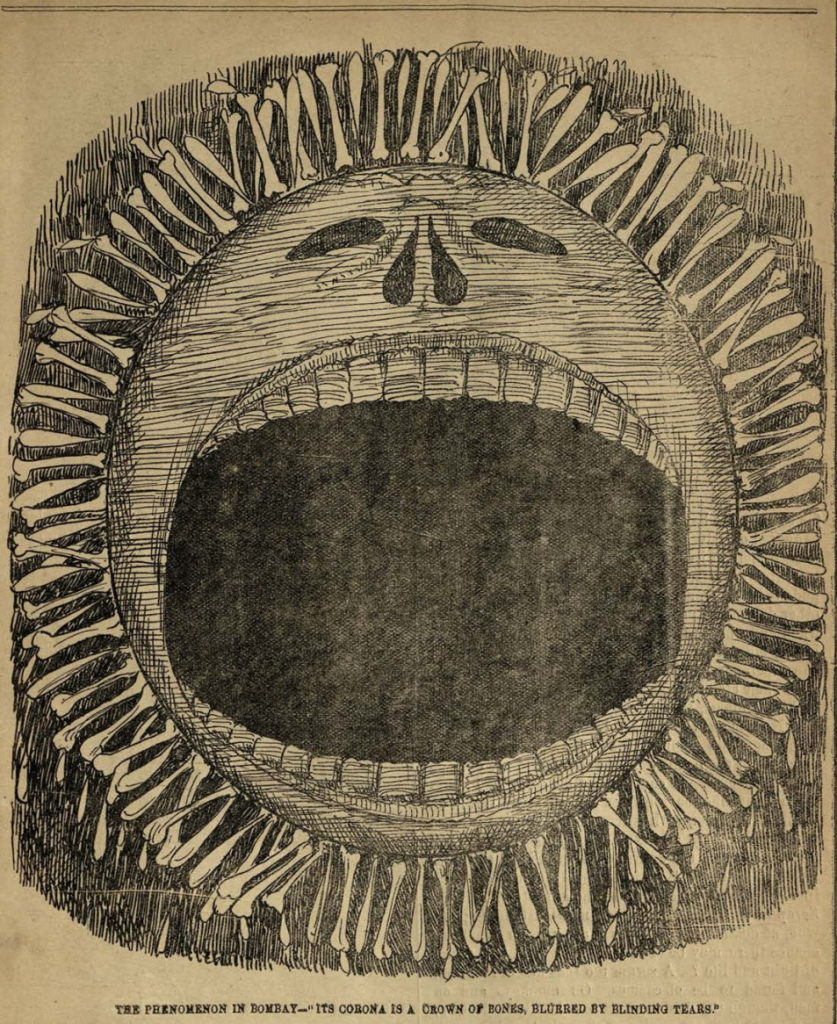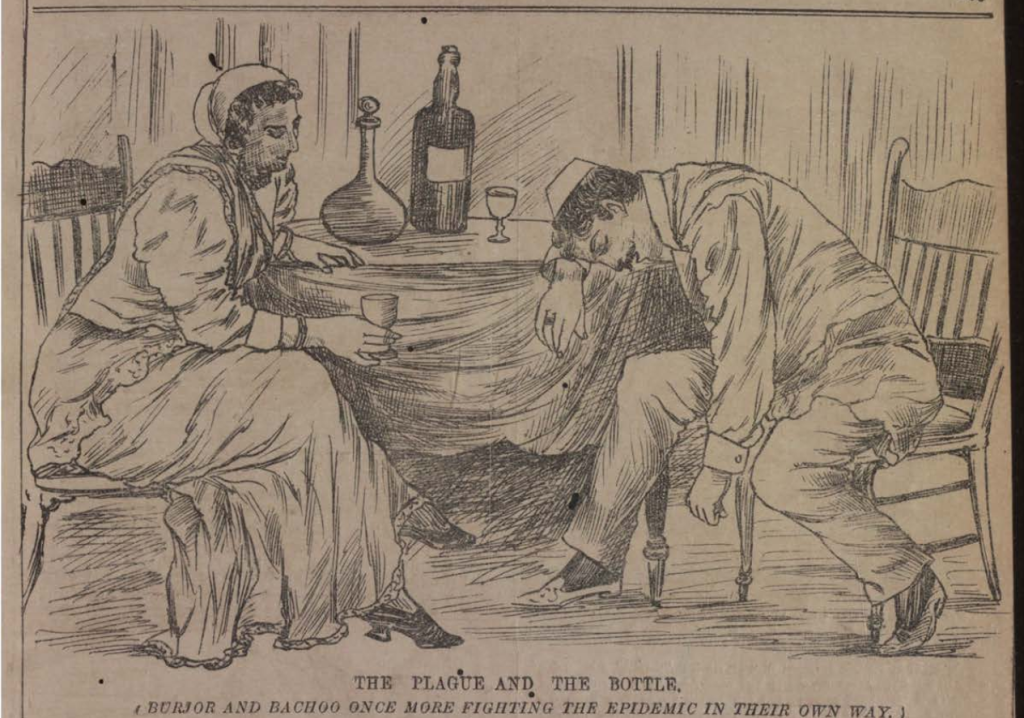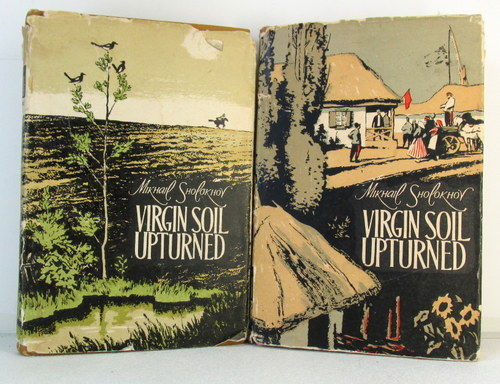काम-चिंतन की कणिकाएँ: रामधारी सिंह दिनकर
(१)
बहुत-सी नारियाँ इस भ्रम मे रहती हैं कि वे प्यार कर रही हैं। वास्तव मे वे प्रेम किये जाने के कारण आनन्द से भरी होती हैं। चूँकि वे इनकार नहीं कर सकती, इसलिए यह समझ लेती हैं कि हम प्रेम कर रही हैं। असल में यह रिझाने का शौक है, हलका व्यभिचार है । प्रेम का पहला चमत्कार व्यभिचार को खत्म करने में है, पार्टनर के भीतर सच्चा प्रेम जगाने में है !
(२)
ऐसी ओरतें हैं, जिन्होंने प्रेम किया ही नहीं है । लेकिन ऐसी औरतें कम हैं, जिन्होंने प्रेम केवल एक ही बार किया हो ।
जब प्रेम मरता है, तब बची हुई चीज ग्लाति होती है, पश्चात्ताप होता है।
प्रेम आग है, जलने के लिए उसे हवा चाहिए। आशा और भय के समाप्त होते ही प्रेम समाप्त हो जाता है ।
सुखमय विवाहित जीवन सम्भव है। स्वादमय विवाहित जीवन सम्भव नहीं है ।
प्रेम का नाम नहीं सुनते, तो बहुत-से लोग हैं, जो प्रेम में नहीं पड़ते। कवियों और उपन्यास-लेखकों ने प्रेम का प्रचार किया है ।
(३)
औरतें अपनी वासना को काबू में ला सकती है, मगर अपनी रिझाने की प्रवृत्ति को वे रोक नहीं सकती ।
प्रेम में पागल हो जाना किसी हद तक ठीक है, बेवकूफ बनना बिलकुल ठीक नहीं है ।
(४)
ऐसी सती नारियाँ कम हैं, जो अपने जीवन को बेस्वाद नहीं मानती हो । ये नारियाँ उस खजाने के समान हैं, जो सुरक्षित इसलिए है क्योकि वह गड़ा हुआ है। यानी इसलिए कि उसका पता किसीको चला ही नहीं है । ज्यों-ज्यों नर-नारी के मिलन के अवसरों मे वृद्धि हुई है, त्यों-त्यों सती नारियों की संख्या में हास हुआा है “पुरानी नैतिकता तभी बचायी जा सकती है, जब नर और नारी के मिलन के अवसर कम कर दिये जायें । नारी अग्नि है, पुरुष घृत-कुंभ है । दोनों के अलग रहने में ही पुरानी नैतिकता का कल्याण है ।
(५)
आदि काण्ड में नारी प्रेमी से प्रेम करती है । उसके बाद वह प्रेमी से नहीं, प्रेम से प्रेम करने लगती है ।
प्रेम और सतर्कता, ये साथ नहीं चल सकते । जैसे-जैसे प्रेम में वृद्धि होती है, सतर्कता खत्म होने लगती है ।
(६)
जो समाज अपनी औरतों को परदो में बन्द रखता है और जो समाज उन्हें घुमने-फिरने की आजादी देता है, उन दोनों की कविताएँ अलग-अलग ढंग की होगी ।
सुन्दरता के बारे में तर्क जितना ही अधिक किया जायेगा, उसकी अनुभूति उतनी ही कम होगी।
(७)
सुखी प्रेम का इतिहास नहीं होता । प्रेम का इतिहास रोमांस का इतिहास है और रोमांस तब जन्म लेता है, जब प्रेम में वाधा पड़ती है, रुकावट आती है, विशेषतः तब, जब प्रेम दुखांत होता है। जिस प्रेम में आतुरता है, तेजी है, छटपटाहट और बेचैनी है, वह विपत्ति लाकर रहेगा ।
कहते हैं, यूरोप और अमरीका में व्यभिचार सबसे बड़ी प्रवृत्ति है । व्यभिचार न हो, तो कविता और उपन्यास में क्या रह जाता है ? सारा साहित्य उस प्रेम के इर्द-गिर्द चक्कर काटता है, जो नियमों का पालन करना नहीं जानता । मनुष्य जाति की आधी से अधिक विपत्तियों का नाम व्यभिचार है ।
विवर्जित के प्रति आकर्षण है, इसलिए विवाह टूटते हैं। लेकिन विवर्जित के प्रति आकर्षण में दुख है, यह जानते हुए भी आदमी संत्रास को स्वेच्छया क्यों अपनाता है ?
(8)
प्रेमी अपराध करके न तो सुधार की शोशिश करते हैं, न पश्चाताप । कारण ? उनका अंतर्मन कहता है कि उन्होंने पाप नहीं किया है, पाप और पुण्य की सीमा को लाँघकर वह आनन्द लूटा है, जो आनन्द पाप और पुण्य की सीमा के इघर है ही नहीं । अवैध प्रेम में प्रेम की पात्री नायिका नहीं होती, बल्कि यह अनुभूति होती है कि हम प्रेम कर रहे हैं। नारी नर को और नर नारी को इसलिए नहीं चाहता कि वे नर और नारी है, बल्कि इसलिए कि दोनों के मिलते ही एक ज्वाला उठती है, जो केवल नर या केवल नारी में नहीं उठ सकती।
रुकावट के बिता प्रेम मे जोर नहीं आता, रोमांस की आग नहीं धधकती। जहाँ असली रुकावट नहीं है, वहाँ उसकी कल्पना कर ली जाती है। प्रेमियों के प्रति दया हमारे भीतर यह सोचकर आनी चाहिए कि अन्त में विषाद उनका
इंतज्ञार कर रही है ।
वासना शरीर का चाहे जितना भी उपयोग करे, किन्तु शरीर के कानून को तोड़कर वह जीवित नहीं रह सकती । यूनानी और रोमन लोग इसीलिए प्रेम को बीमारी समझते थे।
(९)
वासना को शब्द और भाषा साहित्य से मिली है। अगर साहित्य ने प्रेम पर इतनी बातें नहीं कही होती, तो कम लोग इस जजाल में फँसते। गेटे के वर्दर (The Sorrows of Young Werther) के प्रकाशन के बाद यूरोप में आत्महत्या की लहर आ गयी थी। रूसो के प्रभाव में आकर लोग दूध ज्यादा पीने लगे थे। रेने के प्रकाश में आने के बाद कई पीढियाँ गमगीन रही थी । सुना है कि एक बार कलकत्ते में एक फिल्म का इतना भयानक प्रभाव पड़ा कि कई लड़कियों ने झील मे कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उस फिल्म का नाम देवदास था।
(१०)
मैं तो भाग्य की ठोकरे खाकर अध्यात्म की ओर मुड़ा हूँ, मगर यह देवी शायद सुख से ऊबकर अध्यात्म की ओर जा रही है। लेकिन वह अभी काम और अध्यात्म के बीच झटके खा रही है, कोई ऐसा मार्ग खोज रही है, जो अध्यात्म का मार्ग हो, लेकिन काम का विवर्जन उससे नहीं होता है । अध्यात्म की सुनी-सुनायी बातें वह जोर से दुहराती रही और खोद-खोदकर यह पूछती रही कि विवाह-बाह्य प्रेम हो जाय, तो पाप उसे क्यों माना जाना चाहिए। मालूम होता है, उसे जब कोई युवक अच्छा लगता है, तब इतने से ही यह द्वंद्व उसे सताने लगता है ।
वह पूछने लगी, एक नारी दो नरों को प्यार कर सकती है या नहीं ? एक नर दो नारियों को प्यार कर सकता है या नहीं ? मन वो आप से आप खिंच जाता है उसे समेटे तो कैसे ? और यह समेटना ही क्या पुण्य है ? लड़की का हाथ मैं अपने हाथ मे ले सकती हूँ । लड़के का हाथ अपने हाथ में लेने से मन क्यों घबराता है ? बीहड़ प्रश्न ।
मैंने कहा, यूरोप में चूमना भी दोष नहीं माना जाता । भारत में मात्र हेरने से शंका उत्पन्न हो जाती है । द्वंद्व व्यक्ति की तरंग और समाज के नैतिक बन्धन का है । अध्यात्म के बारे में मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता, लेकिन धर्म तो खुल्लम-खुल्ला समाज के नैतिक विधान के पक्ष में है। मगर अब मनोविज्ञान का राज चलने लगा है। मनोविज्ञान की शिक्षा है कि जान-बूझकर फैलने की कोशिश मत करो, जान-बूझकर सिकुड़ने की भी कोशिश मत करो । लेकिन याद रखो कि बार-बार की परीक्षाओं के बाद भी विवाह की प्रथा सही पायी गयी है और विवाह के अपने कानून हैं। जिस बात से पति या पत्नी को शंका हो, चिन्ता हो, शिकायत हो, वह बात चल नहीं सकती ।
मुश्किल यह है कि अब मिलने-जुलने के इतने साधन निकल आये हैं कि पुरानी नैतिकता के लिए संकट खड़ा हो गया है। और जो नैतिकता इस नयी दुनिया से मेल खाती है, वह नैतिकता है ही नहीं । उपन्यासों में सेक्स की समस्या का चित्रण जिस रूप में किया जा रहा है, उससे तो यही शिक्षा निकलती है कि पति और पत्नी को परस्पर सहनशील होना चाहिए । जिस नाव में औरत बैठी है, उसी नाव में मर्द भी है।
देवी ने पूछा, “इस विपय मे श्री अरविन्द की राय क्या है ? ”
मैंने कहा, “उनका निश्चित मत था कि उनका योग नर-नारी-समागम के साथ चल नहीं सकता । श्री अरविन्द आश्रम में सेक्स की मनाही है। लेकिन ‘ईव्निंग टॉक’ में कहीं उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था कि नर-नारी-सम्बन्ध का विषय अत्यन्त निगूढ़ है। उसे तुम अभी नहीं, आगे चलकर समझोगे। श्री अरविन्द से किसीने पर-स्त्री-गमन के विषय में भी पूछा था। उन्होंने कहा, “यह तो अपनी स्त्री के साथ समागम से भी खराब है ।”
इसके विपरीत, महर्षि रमण ने एक भक्त के बार-बार के प्रशन से आजिज होकर कहा था, “अगर तुम इस विषय में निरन्तर सोचते रहना नहीं छोड़ सकते, तो अच्छा है कि कर ही डालो और इस बार-बार के सोचने से मुक्त हो जाओ।”
मैंने कहा, “मन का सेक्स बहुत ही खराब चीज़ है, तन का सेक्स उतना बुरा नहीं माना जा सकता ।”
देवी ने इस सूक्ति को नोट कर लिया। मैंने अपने जीवन का एक अनुभव उसे सुनाया और कहा कि उस महिला को मैं हमेशा पवित्र मानता आया हूँ ।
मैंने उसके मन पर यह बात बिठाने की कोशिश की कि अध्यात्म का मार्ग ठीक-ठीक वही मार्ग नहीं हो सकता, जिस पर विषयी लोग चलते हैं । दूसरों के स्खलन के प्रति उदार रहो, मगर खुद स्खलन से बचो, यही संतों का दृष्टिकोण है।
(११)
बारहवीं सदी में फ़्रांस में प्रेम आदर का विषय था और प्रेमी इज्जत से देखे जाते थे । इसी कारण साहित्य में एक परम्परा बन गयी, जिसका वर्तमान रूप यह है कि नैतिकता की दृष्टि से वासना उत्तम वस्तु है। वासना के लिए यह तनिक भी आवश्यक नहीं है कि वह सामाजिक रस्म-रिवाज या आचरण का ध्यान रखे । जो भी व्यक्ति उद्दामता के साथ प्रेम करता है, वह औसत आदमियो के झुंड में से उठकर उन उन्नत लोगो के बीच पहुँच जाता है, जिनकी संख्या थोड़ी है और जो पाप और पुण्य के पचड़े से निकल गये हैं। यही परम्परा अब सिनेमा में घुसकर ध्वंस फैला रही है। वासना पुण्य और पाप से अलग स्वतन्त्र अनुभूति का विषय बन गयी है और सिनेमा से शिक्षा यह निकल रही है कि प्रेम आचारों से मुक्त होता है। लेकिन यह मुक्ति नहीं है। आदमी मुक्त तभी होता है, जब इन्द्रियाँ उसके वश में आ जाती हैं।
सिनेमा और साहित्य का सस्ता सुयश यह बतलाता है कि मानवता प्रेम के मारे बीमार है ।
(१२)
रोमांटिक मर्द किस नारी की ओर जाना चाहता है ? उस नारी की ओर, जो सभी नारियों में छिपी विचित्रता का सार है, जो आकर भी नहीं आती है, जो आलिंगन में बंधने पर भी स्पर्श से दूर है, जो आकांक्षा जगाकर उसे तृप्त करने से भागती है, जो शय्या में होकर भी पूर्ण रूप से वहाँ नही होती, “जो सपने के सदृश बाँह में उड़ी-उड़ी आती है; और लहर-सी लौट तिमिर में डूब-डूब जाती है।”
“प्रियतम को रख सके निमज्जित जो अतृप्ति के रस में;
पुरुष बड़े सुख से रहता है उस श्रमदा के वश में।”
(१३)
नर और नारी अपने माशूक को अवैध मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, जिससे उन्हें प्रेम के लिए प्रेम का सुख मिल सके । आनन्दातिरेक भी अब एक तरह की सनसनाहट का नाम हो गया है। उसकी कोई मिल नहीं है, कोई दिशा नहीं है।
जो लोग तुलना के भ्रम में पड़े हुए हैं। मेरी बीबी वैसी नहीं हैं, जैसी दूसरे की बीबी । अरे यार, औरत को कमर तक ढँक दो, फिर सभी औरतें बराबर हैं। और भावना चाहो, तो वह कुरूप नारी में भी मिलती है। रूप के न होने पर भी प्रेम व्यर्थ नहीं होता । प्रेम व्यर्थ होवे रूप बिना ?
अगर हर कोई अपने पति या अपनी पत्नी से अतृप्त हो, तो समाज का रूप क्या होगा ?
वे जानते नहीं कि जो कुछ उनके पास है, उसका आनन्द कैसे लिया जाय । आनन्द के कल्पित रूप की खोज में वे फूल-फूल पर मंडराते फिरते हैं। किन्तु आनंद पाने की असली कुंजी उनके पास नहीं है ।
जो सबसे जरूरी चीज है यानी वफादारी, उसीको वे कहीं खो आये हैं। वफादारी के मानी ये हैं कि हम अपने पार्टनर को उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ स्वीकार करते हैं, प्रेम को बीच में लाये बिना हम उसे मनुष्य के रूप में ग्रहण करते हैं।
रूस के निहिलिस्ट चिंतक रोमांटिक थे। उन्होंने विवाह की प्रथा को उड़ा दिया था। किन्तु इससे जो बुराइयाँ फैली, उनके खिलाफ लेनिन चिल्लाने लगे और महज सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से विवाह की प्रथा फिर से वापस लायी गयी ।
(१४)
विवाह को आसान मत बनाओ । अमरीका और यूरोप में प्रेम हुआ नहीं कि लड़का-लड़की विवाह कर लेते हैं। यह काफी नहीं है। विवाह की सम्भावनाओं के कारण विवाह होना चाहिए । विवाह सोलह आने प्रेम नहीं है। उसमें कर्तव्य का भी पुट होता है।
समाज के स्थायित्व से अधिक महत्व व्यक्ति के सुख को देना ठीक नहीं है। विवाह के व्रत का जो महत्त्व है, मनोवैज्ञानिक विलास अथवा रेचन के सिद्धान्त का उससे अधिक महत्त्व नहीं हो सकता ।
(१५)
बुद्धि से विवाह की अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती । बुद्धि से ब्रह्मचर्य भी अशक्य व्रत है। उसके लिए अमानुषिक शक्ति चाहिए।
विवाह के प्रस्ताव में यह नहीं कहना चाहिए कि तुम मेरी कल्पना की साकार प्रतिमा हो, तुम मेरी कामनाओं की मूर्ति हो, तुम मेरी लैला हो, जिसका मैं मजनूँ बनना चाहता हूँ। यह कहने से क्या होता है ? कल को मर्दे का मन अगर भर गया, तो पत्नी से उसे कौन सूत्र बाँधकर रखेगा ?
विवाह का उचित प्रस्ताव यह होना चाहिए कि तुम जैसी हो, उसी रूप में मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और वैसे ही स्वीकार करके मैं तुम्हारे साथ रहूंगा । मैं तुम्हें अपनी जीवन-संगिनी बनाता हूँ मेरे प्रेम का यही एकमात्र प्रमाण है ।
आज के नर-नारी की मुद्रा ऐसी हो गयी है कि व्रत को वे आनन्द का शत्रु समझते हैं। व्रत को वे प्राकृतिक नियम नहीं मानते । इसलिए उनकी मान्यता है कि व्रतपूर्ण विवाह अमानुषिक प्रयास के बिना नहीं निभ सकता । जिस आनन्द की वे खोज करते हैं और जीवन का वे जो धर्म समझते हैं, व्रत उसका ठीक प्रतिलोम है। और व्रत को यदि उन्हें पालना ही पड़ा, तो वे समझेंगे कि यह नियम जीवन को अधूरा रखकर ही पाला गया है।
(१६)
छली नायकों के बहाने क्या-क्या हैं ?
“इससे क्या होता है ? यह तो आती-जाती बात है । इससे क्या तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम होता है ?” अथवा यह कि “मैं असमर्थ हूँ । यह मेरी वाइटल जरूरत है । नीतियों की परवाह मैं कैसे करूँ ?” यार, ये ही दलीलें यदि नायिका देने लगें, तो तुम पर क्या गुजरेगी ?
(१७)
अगर औरतें मर्द के बराबर हो गयी, तो उनका डीमोशन हो जायगा। वे मर्दों की खोज व विषय नहीं रह जायेंगी, न पुरुषों की पूजा की पात्री मगर यह बात जरूर है कि प्रेम समानों के बीच होता है और वह समानता को प्रेरित करता है ।
नारी के प्रति हमारा सच्चा प्रेम-निवेदन यह होना चाहिए कि हम उसे समान मानें, मनुष्य मानें और यह सोचना भूल जायें कि नारी चाँदनी है, नारी स्वप्न है, नारी गुलाब और जुही है, वह आधी देवी और आधी कामिनी है। सेक्स और स्वप्न को मिलाकर नारी की रोमांटिक कल्पना रोमांटिक लोगों ने की थी । किन्तु नारी का असली रूप वह है, जिसे या तो मार्क्स ने देखा था या गांधी ने ।
गांधी नर और नारी को व्रती बनाना चाहते थे। पुरुष जब व्रती होता है, तब नारी उसकी दृष्टि मे काम का साधन या प्रतिबिंब नहीं रह जाती, वह व्यक्ति बन जाती है। यह वह दृष्टि है, जो कामियों को ज्ञात नहीं। नारी को मोहक और आमंत्रणपूर्ण मानना अपनी ही कामयुक्त कल्पना का प्रक्षेप है ।
यदि काम तेजी से जिधर-तिधर को भागता फिरे, तो प्रेम की गति मद्धिम रहेगी। प्रेम जब व्रत लेता है और भागीदार के भीतर व्रत की भावना को जन्म देता है, तभी यह कहा जायेगा कि प्रेम ने अपने को पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया ।
जो विवाह में विश्वास करता है, वह प्रथम दृष्टि वाले प्रेम में आस्था नहीं रखता और इस बात में तो बिलकुल ही नहीं कि वासना अदम्य होती है। वासना को अदम्य मानने की जो प्रथा चली है, व्यभिचार को बढ़ावा उसी प्रथा से मिल रहा है।
स्वस्थ ओर शक्तिशाली शरीर वाले लोग प्रथम दृष्टि में प्रेम के शिकार नहीं होते ।
विवाह को भावुकता तथा बर्बर प्रेम का श्मशान मानना चाहिए । यदि बर्बर प्रेम ही प्राकृतिक प्रेम समझा जाय, तो उसकी तगड़ी अभिव्यक्ति बलात्कार में होती है और बलात्कार का अर्थ यह है कि नारी को हम व्यक्ति न मानकर केवल सेक्स की पुतली मानते हैं। बहु-पत्नीत्व और बलात्कार, ये दोनों नारी के व्यक्तित्व का दमन करते हैं ।
सुसंस्कृत और सच्चा प्रेमी कभी भी कोई ऐसा कृत्य नही करेगा, जो हिंसा है, जिससे भागीदार के व्यक्तित्व का ह्रास होता है ।
(१८)
मनोविज्ञान में बहुत-सी फालतू बातों पर भी विचार करते हैं । कहते हैं कि मर्द औरत से इसलिए जलता है कि वह अपने पेट से बच्चा पैदा नहीं कर सकता ।
और औरत मर्द से इसलिए जलती है कि उसके पास लिंग नहीं है, योनि है।
फेमिनिस्ट आन्दोलन वाली औरतें कहती हैं कि औरत-मर्द का भेद प्रकृति ने नहीं किया, वह मर्दों की रची हुई सभ्यता से प्रचलित हुआ है। ओरतें इस सभ्यता को ढाह रही हैं। पोशाक अमरीका में ऐसी चली है, जिसे यूनिसेक्स्वल कहना चाहिए और धन्धे भी औरतें ऐसे करने लगी हैं, जो पुरुषों के हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि पुरुष औरतों से विरक्त हो रहे हैं और नारियाँ समझती हैं कि कोई सन्तोष पुरानी सभ्यता में था, जो उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से नहीं मिल रहा है।
मर्दों के बारे मे कहा जाता है कि वे समलैंगिक हो रहे हैं, विवाह-बाह्य काम का भोग कर रहे हैं। विवाहिता के साथ वे नपुंसक हो गये हैं । और ये ही दोष औरतों में भी उत्पन्न हुए होंगे।
अगर नर-नारी का भेद सभ्यता का किया हुआ है, तो इस सभ्यता को औरतें बर्दाश्त क्यों करती हैं? असली कारण यह है कि जीव-विज्ञान की दृष्टि से औरतों को प्रकृति ने जिस तरह की बना दिया, वे वैसी हो रहेंगी । वे पुरुष को प्यार करने को बनी हैं, पुरुष के द्वारा प्यार किये जाने को बनी हैं। यह स्वभाव नहीं बदलेगा। सामाजिक आचार बदल सकते हैं, मगर वायलाजिकल प्रवृत्ति नहीं बदलेगी । औरतें कहती हैं कि फ्रायड ने औरतों को सहानुभूति से नहीं देखा । इसलिए कि फ्रायड ने कहा था “एनाटामी इज डिस्टिनी ।” शरीर-रचना में जो भेद है, उसीने औरत को मर्द के अधीन बना दिया।
अत्याचार तो औरतों पर हुए हैं। नवीं सदी में जर्मनी में एक कानून था। अगर कोई व्यक्ति कम उम्र की लड़की की हत्या कर देता, तो उसे २०० रुपये जुर्माना होता था। अगर यही हत्या पूर्ण युवा स्त्री की की जाती, तो जुर्माना ६०० रुपये होता था। कारण ? कारण यह कि युवा स्त्री सद्यः उपयोग की वस्तु थी।
अमरीका में कहा जाता है कि प्रभुत्व कायम रखने की कोशिश में औरतें पतियों को पागल बना देती हैं, माताएँ बेटों को आत्महत्या करने को विवश करती हैं। एक लेखिका ने लिखा है, “इसके मानी ये हुए कि अमरीकी औरतें बारी-बारी से पति और पुत्र को खाती हैं ।”
(१९)
दोस्तावास्की के ब्रदर्स कारामाजोव में पिता कहता है कि औरत बदसूरत होती ही नहीं है। जब मैं सबरजिस्ट्रार था, मेरा एक दोस्त कैयूम था। वह डिपुटी मजिस्ट्रेट था। वह भी कहा करता था, खूबसूरत और बदसूरत का भेद बुढ़ापा करता है। जवाती औरत-औरत में भेद नहीं करती ।
सभ्यता जब आदिम अवस्था में थी, मर्द के सबसे प्रथम पालतू जीव का नाम नारी था ।
यूरोप में मध्यकाल में आकर नारी के प्रति भाव बदला । दरबारों में और बड़े घरानों में नारियाँ देवी समझी जाने लगी, प्रेम की देवी, ईश्वर की विभा का प्रतीक । नाइट लोग युद्ध में जाते समय अपनी प्रेमिकाओं का रूमाल साथ ले जाते थे। चुंबन तो किसी-किसी को ही नसीब होता था। मगर यह व्यवहार नाइट अपनी पत्नी से नहीं करते थे, उस नारी से करते थे, जो उनपर मोहित होती थी । या जिस पर वे खुद मोहित होते थे । परन्तु राजपुताने में यह प्रथा नहीं थी। यहाँ प्रेम का चिह्न सामन्त अपनी ही पत्नी से मांगते थे! राणा चुड़ावत ने अपनी महारानी का मूंडमाल ही पहन लिया था।
(२०)
अगर औद्योगिक सभ्यता नहीं आयी होती, तो औरतों को घर के कामों से छुटकारा नहीं मिलता, न वे नारी-स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए समय निकाल पाती । छाती से दूघ पिलाने की प्रथा इसलिए खत्म हो रही है कि औद्योगिक सभ्यता ने शिशुओं के लिए अलग से दूध तैयार कर दिया है।
पश्चिम से जो रिपोर्ट आती है, उससे मालूम होता है कि वहाँ विवाहू-पूर्व अनुभूतियाँ अधिकांश को होती हैं और विवाहितों के भीतर भी व्यभिचार बहुत प्रचलित है। बात कहाँ तक ठीक है, कहना मुश्कित है। पहले की सभ्यता में क्या था, यह जानना भी कठिन है। पहले तो समाज में KINSEY होते नहीं थे !